
नई दिल्ली।2013 की सर्दियों में बीजिंग और दिल्ली—दोनों शहर एक ही तरह की जहरीली हवा में डूबे थे। प्रदूषित धुंध दोनों महानगरों को निगल रही थी। दोनों जगह AQI 500–600 पर था, यानी हवा कम और ज़हर ज़्यादा। लेकिन 2024–25 में नज़ारा बिल्कुल उलट गया। बीजिंग ने अपना AQI लगभग 50-60 तक उतार दिया, जबकि दिल्ली आज भी 500–600 के बीच फँसी है—मानो एक बच्चा एक बार फेल होकर उससे सबक लेकर अगली बार कक्षा में टॉप कर जाए, और दूसरा पिछले 11 साल से बस हर बार नए बहाने ढूँढता रहे।
बीजिंग में 2013 के बाद सरकार ने हवा को साफ़ करने का काम “जुमला प्रोजेक्ट” नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन माना। भारी कोयला आधारित पावर प्लांट शहर से बाहर कर दिए, प्रदूषण करने वाले उद्योगों पर कड़ी कार्यवाही की, निर्माण-स्थलों पर सख़्त धूल नियंत्रण लागू किया, और इलेक्ट्रिक वाहनों(EV), उन्नत सार्वजनिक परिवहन तन्त्र को आम जनता के जीवन में तेज़ी से उतारा। 2013 से 2024 के बीच बीजिंग का PM2.5 स्तर लगभग 60% तक घट गया, और यह किसी चमत्कार से नहीं बल्कि सरकार की सख़्त नीति, जवाबदेही और वास्तविक कार्रवाई का परिणाम था।
बीजिंग में 2013 के बाद जो हुआ, वह किसी साधारण शहर-प्रशासन से ज़्यादा एक सरकार-संचालित “करो या मरो” मॉडल जैसा था। चीन ने पावर प्लांट शहर से बाहर धकेल दिए, कोयले को “राष्ट्रीय खलनायक” घोषित कर दिया, गैसिफिकेशन लागू किया, भारी उद्योग शहर से दूर कर दिए, और कोई फैक्टरी नियम तोड़े तो सीधी सीलिंग कर दी गई। ये बातें हवाई नहीं, WHO और कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें हर साल यही कहानी दोहराती हैं। चीन ने जिस तरह EVs, निर्माण-धूल नियंत्रण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया, उसे देखकर लगता है कि सरकार ने साफ़ हवा को राष्ट्रनिर्माण का हिस्सा मान लिया था।
अब दिल्ली की ओर देखिए। यहाँ हवा सफ़ाई से ज़्यादा “सरकारी बयानबाज़ी” से चलती है। 2013 में AQI 500–600 था, और 2025 में भी वही। हर साल धुआँ दिल्ली के आसमान को घेर लेता है, लेकिन समाधान? सरकार हर साल नई घोषणाएँ करती है, समितियाँ बनती हैं, ऐप लॉन्च होते हैं—पर ज़मीनी स्तर पर वही ढाक के तीन पात।
सरकारों के लिए पराली जलाने की समस्या पर ठीकरा फोड़कर किसानों को ज़िम्मेदार ठहराना सबसे आसान होता है, जबकि आंकड़ों के अनुसार इसका योगदान औसतन 10–12% तक ही रहता है। बाकी प्रदूषण वाहनों, फैक्ट्रियों और निर्माण कार्यों से उठने वाले धूल-धक्कड़ का है।
अगर पराली के धुएँ के कारणों की बात करें, तो सरकारें हर साल प्रेस कॉन्फ़्रेंस करती हैं, स्मॉग टावर बनाती हैं (जो हवा साफ़ करने की बजाय बस फोटो साफ़ करते हैं), मगर किसानों के पास आज भी न प्रदूषण-रहित मशीनें हैं, न सस्ती तकनीक, न पर्याप्त आर्थिक सहायता। ऊपर से महंगे खाद, बीज, बिजली और निष्प्रभावी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की नीतियाँ ऐसी कि किसान के पास पराली जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। और जब पराली जलती है, तो दिल्ली की जनता को सरकारों की नाकामी का धुआँ फेफड़ों में भरकर पीना पड़ता है—यानी प्रदूषण की जिम्मेदारी भी किसानों पर डालकर पल्ला झाड़ लिया जाता है: गरीब किसान को दोष, अमीर उद्योगों को छूट, और जनता को दम घोंटने की पीड़ा।
दिल्ली केवल खेतों के धुएँ से नहीं घिरती। NCR देश का सबसे बड़ा निर्माण-क्षेत्र है, जहाँ धूल ऐसे उड़ती है मानो उसको रोकने की माँग करने का मतलब “विकास विरोधी” होना हो। ऊपर से 1 करोड़ से अधिक वाहन, जिनमें Electric Vehicle (EV) की हिस्सेदारी आज भी बेहद कम है। हर कार, हर फैक्ट्री, हर निर्माण स्थल मिलकर दिल्ली की हवा को ऐसा जहरीला मिश्रण बना देते हैं कि WHO के शोधकर्ता भी इसे देखकर घबरा जाएँ। और कानून? भारत में कानून सिर्फ़ गरीबों को पीड़ित करने के लिये होते हैं, अमीरों के लिये ज़ेब में रखने की चीज।
दिल्ली में सार्वजनिक स्वास्थ्य लगातार टूट रहा है—बच्चों के फेफड़े कमजोर हो रहे हैं, बुज़ुर्गों को साँस लेने में दिक्कत हो रही है, स्कूलों को बार-बार बंद करना पड़ता है। लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया वही पुरानी—“निगरानी जारी है।”
यह वही व्यवस्था है जहाँ जनता की ज़रूरतें पीछे धकेल दी जाती हैं और बड़े उद्योगों, निर्माण कंपनियों और निजी मुनाफ़े को प्राथमिकता दी जाती है। जब सरकार अपनी नीति को जनता-केंद्रित नहीं बल्कि मुनाफ़ा-केंद्रित बनाती है, तब हवा भी उसी राजनीति का शिकार बनती है।
बीजिंग ने साबित किया कि यदि सरकार सच में चाहे, तो 10–12 साल में हवा साफ़ की जा सकती है। दिल्ली ने साबित किया कि यदि सरकार इच्छा न दिखाए, तो 50 साल में भी हवा जस की तस रह सकती है।
ऐसा नहीं है कि बीजिंग में कोई जनवादी सरकार है—वहाँ भी पूँजीवादी नीतियाँ ही आगे बढ़ती हैं—लेकिन समाजवादी दौर की नियोजित और प्रभावी नीतियाँ लागू करने का अनुभव और इच्छा शक्ति अभी भी उनके पास बची हुई है, खासकर उन मामलों में जहाँ शासक वर्ग भी सीधे तौर पर प्रभावित होता हो। इसी कारण पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, मिलावट आदि के मामलों में वे अब भी कई अन्य सरकारों से बेहतर प्रदर्शन कर लेते हैं।
सच यही है—दिल्ली का प्रदूषण कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि पूरी तरह से सरकारी विफलताओं, मुनाफ़ा-प्रधान नीतियों और जनता की प्राथमिकता की कमी का परिणाम है। 2013 में जो शहर बीजिंग के बराबर खड़ा था, वही 2025 में उससे 10 गुना अधिक प्रदूषित है।
कुल लब्बोलुआब यह है कि जहाँ सरकार जनता को प्राथमिकता देती है, वहाँ हवा भी साफ़ होती है। और जहाँ सरकार लाभ को प्राथमिकता देती है, वहाँ जनता महँगाई, बेरोज़गारी, लचर शिक्षा-स्वास्थ्य व्यवस्था, महिला अपराध, धार्मिक-जातिवादी नफ़रत—साथ ही साफ़ हवा और साफ़ पानी जैसी बुनियादी ज़रूरतों से भी महरूम हो जाती है।
लेख—धर्मेन्द्र आज़ाद
लेटैस्ट न्यूज़ अपडेट पाने हेतु -
👉 वॉट्स्ऐप पर हमारे समाचार ग्रुप से जुड़ें
👉 हमारे फ़ेसबुक पेज को लाइक/फॉलो करें



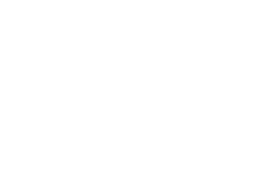 Subscribe Now
Subscribe Now




